In this article, we are providing information about Karak in Hindi – Karak ke bhed | Karak in Hindi Grammar Language. कारक की परिभाषा और भेद उदाहरण सहित, What is karak in hindi
Karak in Hindi Grammar- कारक की परिभाषा और भेद उदाहरण सहित
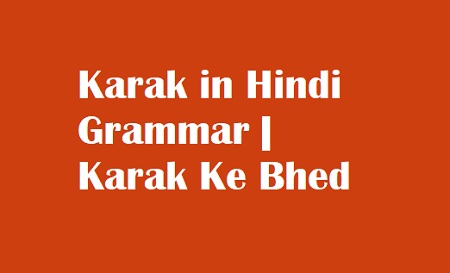
Karak ki Paribhasha | Definition of Karak in Hindi
What is karak in Hindi – संज्ञा या सर्वनाम के उस रूप को कारक कहते हैं जिससे उसका सम्बन्ध वाक्य के अन्य शब्दों विशेषतः क्रिया के साथ प्रकट होता है। वास्तव में, विभक्ति चिह्नों से युक्त संज्ञा या सर्वनाम शब्द ही वाक्य में अन्य शब्दों से सम्बन्ध प्रकट करते हैं।
ने, को, से, द्वारा- आदि विभक्ति चिह्न हैं। कारक का एक उदाहरण इस प्रकार है-‘मोहन ने बाग में डण्डे से आम तोड़ा।’ इस वाक्य में मोहन ने, डण्डे से, और आम संज्ञाओं के रूपान्तरण हैं। जिस तत्त्व के द्वारा इन रूपान्तरित संज्ञाओं का सम्बन्ध तोड़ा, क्रिया से स्पष्ट होता है, वही कारक है।
कारक-चिह्न ( Karak Chinh )
हिन्दी में कारक के आठ भेद माने जाते है :
कारक विभक्ति या कारक चिह्न
1 कर्त ने
2. कर्म को
3. करण से, द्वारा
4.सम्प्रदान को, के लिए
5. अपादान से
6. सम्बन्ध का, के, की, रा, रे, रो, ना, ने, नी
7. अधिकरण में, पर
8. सम्बोधन हे, हो, अरे, अजी, अहो आदि।
कारक-चिह्न/विभक्ति/परसर्ग
हिन्दी में कारक का ज्ञान कराने के लिए संज्ञा या सर्वनाम के साथ जो प्रत्यय लगाये जाते हैं, उन्हें ही व्याकरण में विभक्ति कहते हैं। हिन्दी में चूंकि विभक्ति चिह्न पद से अलग प्रयुक्त होते हैं इसलिए इन्हें परसर्ग’ भी कहा जाता है। परसर्ग का शब्दिक अर्थ है- पीछे जुड़ना। कारक चिह्न सदैव संज्ञा या सर्वनाम के पीछे जुड़ते हैं।
Karak aur Uske Bhed | Karak in Hindi with examples
(i) कर्ता कारक Karta Karak in Hindi – Nominative Case : कर्ता का अभिप्राय है, करने वाला। वाक्य में जो क्रिया सम्पन्न करता है, उसे कर्ता कहा जाता है।
जैसे-
राम पढ़ता है। सुरेश पत्र लिखता है।
इन वाक्यों में राम और सुरेश कर्ता कारक हैं क्योंकि ये ही क्रिया को सम्पादित करने वाले हैं।
(ii) कर्म कारक Karm Karak in Hindi – Instrument Case : कर्ता द्वारा सम्पादित क्रिया का फल जिस पर पड़ता है, उसे ‘कर्म’ कहते हैं।
जैसे-
शीला ने राजेश को पढ़ाया। इस वाक्य में कर्ता है- शीला, क्रिया है- पढ़ाना। पढ़ाना क्रिया का फल राजेश पर स्पष्ट पड़ रहा है। इसलिए यहाँ राजेश कर्म कारक की स्थिति में है।
(iii) कण कारक Karan Karak in Hindi – Ablative Case : वाक्य में कारण कारक उस शब्द को कहते हैं जो क्रिया को पूर्ण करने में साधन के रूप में कर्ता का सहायक होकर आता है।
जैसे-
मैं कलम से लिखता हूँ।
इस वाक्य में ‘कलम से करण कारक है क्योंकि लेखन-क्रिया में कलम साधन है।
(iv) सम्प्रदान कारक Apadan Karak in Hindi – Objective Case : कर्ता क्रिया की सिद्धि जिसके लिए करता है अथवा जिसको कुछ देता है, उसे प्रकट करने वाले शब्द रूप को सम्प्रदान कारक कहते हैं।
जैसे-
श्याम मीरा के लिए खिलौने लाया। राकेश शीला के लिए रोता है।
इन वाक्यों में लाना और रोना क्रियाएँ क्रमशः मीरा और शीला के लिए सम्पादित की जा रही हैं। इसलिए मीरा और शीला केलिए शब्द रूप सम्प्रदान कारक है।
(v) अपादान कारक Apadan Karak in Hindi – Objective Case : वाक्य में अलगाव सूचित करने वाला शब्द अपादान कारक कहलाता है।
जैसे-
शारदा नहर गंगा नदी से निकली है। पेड़ से पत्ते गिरते हैं।
इन वाक्यों में निकलना और गिरना क्रियाओं के अलग होने का भाव क्रमशः गंगा नदी और पेड़ से स्पष्ट हो रहा है। अतएव इन दोनों शब्दों की स्थिति अपादान कारक में है।
(vi) सम्बन्ध कारक Sabandh Karak in Hindi – Dative Case : संज्ञा सर्वनाम का वह रूप जिससे वाक्य में आगत अन्य शब्द के साथ जुड़ाव या सम्बन्ध का बोध हो सम्बन्ध कारक कहलाता है। सम्बन्ध कारक का सम्बन्ध क्रिया के साथ प्रत्यक्ष नहीं होता है।
जैसे-
शीला की पुस्तक। रमेश का घोड़ा। मेरी कलम।
इन वाक्यों में शीला की, रमेश का, मेरी- क्रमशः पुस्तक, घोड़ा, कलम से लगाव स्पष्टकरते हैं। अतः ये सम्बन्ध कारक हैं ।
(vii) अधिकरण कारक Adhikaran Karak in Hindi – Locative Case : संज्ञा या सर्वनाम के उस रूप को अधिकरण कारक कहते हैं जिससे वाक्य में क्रिया के आधार का बोध होता है।
जैसे-
गाय बाग में चरती है। विद्यालय में 400 विद्यार्थी हैं।
इन वाक्यों में ‘बाग में’ और ‘विद्यालय में अधिकरण कारक हैं। क्योंकि वे क्रमशः गाय के चरने के लिए तथा विद्यार्थियों के लिए आधार का काम करते हैं।
(viii) सम्बोधन कारक Sambodhan Karak in Hindi – Vocative Case : वाक्य में वक्ता श्रोता का ध्यान अपनी ओर खीचने के लिए अथवा उसे सचेत करने के लिए संज्ञा के जिस रूप को प्रयुक्त करता है उसे सम्बोधन कारक कहते हैं।
जैसे–
अरे राकेश, तुपने यह क्या हाल कर रखा है।
इस वाक्य में ‘अरे राकेश’ सम्बोधन कारक है, क्योंकि इस रद द्वारा ध्यानाकृष्ट किया गया है। सम्बोधन कारक का सम्बन्ध क्रिया के साथ नहीं होता है। इसका प्रयोग बिना चिह्न के भी हो सकता है। जैसे गुरुदेव, क्षमा करें। यहाँ गुरुदेव सग्बोधन कारक है।
करण कारक और अपादान कारक में अन्तर
करण कारक और अपादान कारक दोनों ही कारकों की विभक्ति ‘से है। किन्तु दोनों में पर्याप्ति अन्तर परिलक्षित होता है। करण कारक उस पद में होता है जो क्रिया को सम्पादित करने म साधन के रूप में कर्ता का सहायक होकर वाक्य में प्रयुक्त होता है। जैसे- राम ने बाण से रावण को मारा।
इस वाक्य में ‘बाण’ करण कारक की अवस्था में है, क्योंकि बाण की सहायता से राम ने रावण के मारने के कार्य को पूर्णता प्रदान की। दूसरी ओर अपादान कारक उस पद में होता। है जो वाक्य में पार्थक्य सूचित करता है। जैसे- गंगा हिमालय से निकलती है। यहाँ गंगा के निकलने का काम हिमालय से हो रहा है, अतः हिमालय अपादान कारक के रूप में वाक्य में प्रयुक्त हुआ है।
कर्म और सम्प्रदान कारक में अन्तर
हालाँकि कर्म और सम्प्रदान कारक दोनों की ही विभक्ति ‘को’ है तथापि दोनों के प्रयोग में अन्तर है। कर्म कारक वाक्य में प्रयुक्त उस पद में होता है जिस पर कर्ता द्वारा की गयी क्रिया का फल पड़ता है। जैसे- मैंने महेश को पढ़ाया। वाक्य में क्रिया का कर्ता ‘मैं’ है और क्रिया‘पढ़ाना’ । पढ़ाना क्रिया के कर्ता का फल ‘महेश’ पर पड़ रहा है। इसलिए ‘महेश’ कर्म कारक है। सम्प्रदान कारक में कर्ता जिसके लिए क्रिया का सम्पादन करता है अथवा जिसको कुछ देता है, उसे प्रकट करने वाले शब्द को सम्प्रदान कारक की स्थिति में माना जाता है। जैसे- मैं गुड़िया के लिए खिलौने लाया। इस वाक्य में लाया क्रिया को ‘गुड़िया’ के लिए पूरा किया गया। अतः ‘गुड़िया’ सम्प्रदान कारक है।
‘ने ‘ का प्रयोग जहाँ-जहाँ होता है।
1 सकर्मक क्रियाओं में सामान्य भूत, आसन्न भूत, पूर्ण भूत, संदिग्ध भूत और हेतु हेतु मद् भूत कालों में कर्ता के साथ ‘ने’ प्रयुक्त होता है। जैसे
सामान्य भूत मोहन ने पुस्तक पढ़ी।
आसन्न भूत सोहन ने रोटी खायी है।
पूर्ण भूत शीला ने लिख दिया था।
संदिग्ध भूत शीला ने पुस्तक पढ़ी होगी।
हेतु हेतु मद् भूत उसने पुस्तक पढ़ी होती तो उत्तर दिया होता।
2 यदि क्रिया संयुक्त है और उसके दोनों खण्ड सार्थक हैं तो ऊपर कथित कालों में कर्ता के साथ ‘ने आता है।
जैसे- बेबी ने लिख दिया। अंजु ने कहला भेजा है। आदि।
3 संयुक्त क्रिया का उत्तर खण्ड यदि सकर्मक है तो ऊपर कथित भूतकाल के भेदों में कर्ता के आगे ‘ने’ का प्रयोग होगा।
जैसे- मैंने रो दिया।
4. छींकना, थूकना, नहाना, भेंकना, आदि अकर्मक क्रियाओं में कर्ता के साथ भी उपर्युक्त भूतकालों में ‘ने का प्रयोग होता है।
जैसे- राम ने छींका।
मोहन ने थूका था।
अमित ने नहाया था।
कुत्ते ने भौंका होगा।
5. प्रेरणार्थक क्रिया में अपूर्णभूत के अतिरिक्त भूतकाल के सभी कालों में कर्ता के साथ ‘ने’ आता है।
जैसे- राम ने पुस्तक दिलवायी।
6. वाक्य में यदि अकर्मक क्रिया सकर्मक के रूप में प्रयुक्त होती है तो उपर्युक्त भूतकालों में कर्ता के साथ ‘ने’ चिह्न आता है।
जैसे- चन्द्रगुप्त मौर्य ने अनेक लड़ाइयाँ लड़ी हैं।
7. संयुक्त क्रिया के अन्त में यदि ‘डालना’ या ‘देना’ क्रिया आती है तो सामान्य भूत, आसन्न भूत, पूर्णभूत और संदिग्ध भूत कालों में कर्ता के साथ ‘ने’ चिह्न आता है।
जैसे- शेर ने शिकार को मार डाला।
‘ने का प्रयोग जहाँ-जहाँ वर्जित है।
1. संयुक्त क्रिया का दूसरा खण्ड यदि अकर्मक हो तो कर्ता के साथ ‘ने का प्रयोग नहीं होता है। जैसे- मोती सारा दूध पी गया।
2. अकर्मक क्रियाओं के भूतकाल में कर्ता के आगे ‘ने’ परसर्ग का प्रयोग नहीं होता है। जैसे वह रोया। पत्ता गिरा।
3 पूर्ण कालिक क्रियाओं में कर्ता के साथ ‘ने का प्रयोग नहीं हो सकता। जैसे- नरेश पढ़कर सो गया।
4. जाना, सकना और चुकना क्रियाओं के भूतकाल में कर्ता के साथ ‘ने’ चिह्न नहीं आता है। जैसे- मैं पढ़ चुका। वह जा सका।
‘को’ का प्रयोग जहाँ-जहाँ होता है।
1 ‘को’ विभक्ति का प्रयोग कर्मकारक में होता है। जैसे- सपेरे ने साँप को पकड़ा। मोहन ने पुस्तक को खरीदा।
2. सम्प्रदान कारक में भी ‘को’ विभक्ति प्रयुक्त होती है। जैसे- विद्यार्थियों ने शिक्षक को लेखनी और डायरी दी।
3 वाक्य में यदि द्विकर्मक क्रिया का व्यवहार होता है तो प्राणिवाचक कर्म के साथ ‘को’ क प्रयोग किया जाता है। जैसे- राजा ने ब्राह्मणों को धन दिया।
4. जब विशेषण का प्रयोग कर्म के रूप में होता है तो उसके साथ भी ‘को’ का व्यवहार होता है। जैसे- मूर्खा को उपदेश देना व्यर्थ है। गरीबों को सताना नहीं चाहिए।
5. यदि मानसिक आवेगों को स्पष्ट किया जाता है तो कर्ता के साथ ‘को’ आता है। जैसे- तुम को आनन्द मिल रहा है। राम को ईष्र्या हो रही है।
6. प्रेरणार्थक क्रिया के साथ, गौण कर्म के साथ ‘को’ चिह्न का व्यवहार होता है। जैसे- गरु शिष्य को पुस्तक पढ़ाता है।
7. कै, दस्त, पेशाब, टट्टी आदि स्वाभाविक आवेगों को व्यक्त करने के लिए कर्ता के साथ | ‘को’ का प्रयोग होता है। जैसे- सुरेश को दस्त आ रहे हैं। उसको पेशाब करने जाने दो।
8. व्यक्तिवाचक, अधिकारवाचक एवं सम्बन्धवाचक कर्म में ‘को’ 3ाता है। जैसे- आप राम को पहचानते हैं। (व्यक्ति वाचक वाक्य) मैं अपने पुत्र को भेजता हूँ। (अधिकार वाचक वाक्य) मालिक नौकर को बुलायेंगे। (सम्बन्ध वाचक)
9. मन, जी, आदि के साथ भी ‘को’ का प्रयोग होता है। जैसे- अंग्रेजी में एम. ए. करने को मन करता है। कहानी लिखने को जी होता है। 10. अधिकरण कारक के स्थान में ‘को’ का प्रयोग होता है। जैसे- मैं रात को गया था।
11. समझना, बनाना, मानना, करना आदि अपूर्ण क्रियाओं के साथ जो कर्म है और यदि उन क्रियाओं की कर्मपूर्ति विद्यमान होती है तो उसके साथ ‘को’ का प्रयोग होता है। जैसे- मैंने रमेश को महाविद्यालय का प्राचार्य बनाया। तुमने उसको गलत समझा।
‘को’ का प्रयोग जहाँ-जहाँ वर्जित है।
1 अप्राणिवाचक शब्दों के साथ ‘को’ का प्रयोग नहीं होता है। जैसे- वह रामायण पढ़ता है।
2 छोटे-छोटे जीवों के साथ भी ‘को’ नहीं आता है। जैसे- छिपकली तिलचट्टा पकड़ती है।
3 यदि कर्म अनिश्चित या अपरिचित होता है तो को’ का प्रयोग नहीं होता है। | जैसे- सेठजी एक नौकर खोजते हैं। राम ने हाथी देखा।
4. सजातीय कर्म में ‘को’ नहीं आता है। जैसे- प्रताप ने मुगलों से कई लड़ाइयाँ लड़ीं।
5. द्विकर्मक क्रिया में कर्म के साथ ‘को’ का प्रयोग नहीं होता है। जैसे- मैंने तुमको पुस्तक दी।
‘से का प्रयोग जहाँ-जहाँ होता है।
1 क्रिया सम्पादित करने के साधन के अर्थ में ‘से’ का प्रयोग होता है। जैसे- मैं लेखनी से लिखता हूँ।
2. पहचान के अर्थ में ‘से’ का प्रयोग होता है। जैसे- वह भाषा से मराठी लगता है।
3. कर्मवाच्य, भाववाच्य और प्रेरणार्थक क्रियाओं में कर्ता के साथ ‘से’ का व्यवहार होता है। जैसे- पुस्तक राम से पढ़ी गयी।मुझसे चला नहीं जाता। तुम सुनीता से पुस्तक पढ़वाओ।
4. प्रकृति या स्वभाव के अर्थ में ‘से’ प्रयुक्त होता है। जैसे- तन से मोटा। स्वभाव से उदार। हृदय से कोमल।
5. करण के अर्थ में ‘से’ प्रयुक्त होता है। | जैसे- गुड़िया के जाने से बड़ा दुःख हुआ।
6. रीति के अर्थ में ‘से’ का प्रयोग होता है। जैसे- विद्यार्थी क्रम से बैठे हैं।
7. वाक्य में प्रयोज्य कर्ता के साथ ‘से’ चिह्न आता है। जैसे- रमेश कौशल से पत्र लिखवाता है। वाक्य में कौशल प्रयोज्य कर्ता है और वास्तविक कर्ता रमेश है।
8. गौण कर्म के स्थान में ‘से’ का प्रयोग होता है। जैसे- वह तुमसे क्या पूछ रहा था? उसने मुझसे कहानी सुनी।
‘से का प्रयोग जहाँ-जहाँ वर्जित है।
भूख, प्यास, जाड़ा, गर्मी, हाथ, आँख इत्यादि का प्रयोग जब बहुवचन में होता है, तब इन शब्दों के साथ ‘से’ विभक्ति का प्रयोग नहीं होता है। जैसे- किसान भूखों मर गये।
अपादान कारक में ‘से’
1.अलगाव का अर्थ होने पर अपादान कारक में ‘से’ का प्रयोग होता है। जैसे- दिल्ली से पत्र आया। पेड़ से फल गिरते हैं।
2. उत्पत्ति के अर्थ में ‘से’ का प्रयोग होता है। जैसे- नहर नदी से निकलती है। खेतों से अन्न उपजता है।
3. समय या काल, स्थान आदि की दूरी स्पष्ट करने के लिए भी ‘से’ का प्रयोग होता है। जैसे- कानपुर से दिल्ली अधिक दूर नहीं है। वह विगत सोमवार से बीमार है।
4. तुलना के अर्थ में ‘से’ का प्रयोग होता है। जैसे- राम मोहन से लम्बा है।
5. हीनता का बोध कराने के लिए भी ‘से’ का प्रयोग होता है। जैसे- रश्मि मनीषा से कमजोर है।
‘में’ का प्रयोग
1अधिकरण कारक में ‘में’ चिह्न का प्रयोग होता है। इस अवस्था में ‘में आधार का बोध कराता है। जैसे- नदी में जल है।
2. समय का बोध कराने के अर्थ में भी ‘में’ का प्रयोग होता है। जैसे- मैं दिन में नहीं सोता हूँ। राकेश रात में पाठ याद करता है।
3. निर्धारण के अर्थ में ‘में प्रयुक्त होता है। जैसे- संतों में कबीर श्रेष्ठ ।
4. घृणा, प्रेम, बैर, मित्रता, अन्तर आदि भावों को स्पष्ट करने के लिए भी ‘में’ का प्रयोग होता है। जैसे- राधा और मीरा में बहुत अन्तर है। रमेश और कमलेश में मित्रता है।
5. स्थिति स्पष्ट करने के लिए भी ‘में’ का प्रयोग किया जाता है। जैसे- वह कष्ट में है।
पर” का प्रयोग
1, ‘पर’ अधिकरण कारक का विभक्ति चिह्न है। इसका प्रयोग ‘ऊपर’ के अर्थ में किया जाता है। जैसे- वृक्ष पर पक्षी बैठे हैं।
2. नियम पालन का बोध कराने के लिए ‘पर’ का प्रयोग किया जाता है। जैसे- अपनी बात पर अटल रहना चाहिए।
3. कारण स्पष्टीकरण के अर्थ में ‘पर’ का व्यवहार किया जाता है। जैसे- वह मेरे पहुँचने पर अत्यन्त प्रसन्न थी।
4. निश्चित समय का संकेत करने के अर्थ में भी ‘पर’ का प्रयोग होता है। जैसे- वर्षा बोआई पर प्रारम्भ हुई।
5. मूल्य बताने के अर्थ में भी ‘पर’ का व्यवहार किया जाता है। इसका अभिप्राय के लिए लिया जाता है। जैसे- अधिकारी रुपयों पर बिकने लगे हैं।
संज्ञाओं की कारक रचना
1. यदि कारक की विभक्ति का प्रयोग हो तो संस्कृत से भिन्न आकारान्त पुल्लिग संज्ञाओं के वचन में अंतिम आकार को एकार में परिवर्तित कर देते हैं। जैसे-
बकरा — बकरे ने, बकरे को, बकरे से
घोड़ा — घोड़े ने, घोड़े को, घोड़े से ।
2. संस्कृतेतर शब्दों में विभक्ति का प्रयोग होने पर संज्ञाओं के बहुवचनात्मक रूपों के साथ ‘औ’ तथा ‘यों’ प्रत्यय जोड़ते हैं। जैसे-
गधे — गधे ने, गधों को, गधों से।।
लड़कियाँ — लड़कियों ने, लड़कियों को, लड़कियों से।
3. हिन्दी शब्दों के अन्त में यदि ‘ओं पहले से विद्यमान होता है तो उसका कारकीय रूप बहुवचन में ज्यों का त्यों बना रहता है। जैसे- सरसों ने, सरसों को।
4. ह्रस्व या दीर्घ इकारान्त शब्दों को कारक का बहुवचन रूप बनाने के लिए अन्त में “यों का प्रयोग करते हैं। साथ ही ईकारान्त शब्दों के अन्त में ‘यों जोड़ने के पूर्व ई’ को ‘इ’ बना देते हैं। जैसे
ऋषि ऋषियों ने ऋषियों को।
मति मतियों ने मतियों को।
डाली डालियों ने डालियों को
धनी धनियों ने धनियों को।
5. सम्बोधन कारक की बहुवचन रचना के लिए शब्दान्त में ‘ओ’ जोड़ते हैं। स्मरणीय है, यदि शब्द के अन्त में ‘ई’ या ‘ऊ’ हो तो उसे पहले ह्रस्व कर लेते हैं। जैसे
नर – नरों
माता – माताओं
6. संस्कृतेतर आकारान्त शब्दों का सम्बोधन एकवचन रूप बनाते समय आकार को एकार में बदल देते हैं। जैसे
बच्चा – ए बच्चे।
लड़का – ओ लड़के।
कुछ संज्ञाओं की कारक-रचना
कारक एकवचन बहुवचन
कर्ता नर, नर ने नर, नरों से
कर्म नर, नर को नर, नरों को
करण नर से, नर द्वारा नर से, नरों द्वारा
सम्प्रदान नर के लिए नरों के लिए
अपादान नर से नरों से
सम्बन्ध नर का, के, की नरों का, के, की
अधिकरण नर में, पर नरों में, पर
सम्बोधन हे नर हे नरों
नदी
कारक एकवचन बहुवचन
कर्ता नदी, नदी ने नदियाँ, नदियों से
कर्म नदी, नदी को नदियाँ, नदियों को
करण नदी से, नदी द्वारा नदियों से, नदियों द्वारा
सम्प्रदान नदी के लिए नदियों के लिए
अपादान नदी से नदियों से
सम्बन्ध नदी का, के, की नदियों का, के, की
अधिकरण नदी में, पर नदियों में, पर
सम्बोधन हे नदी हे नदियों
#Karak Hindi Grammar #Examples of Karak in Hindi # Karak chart in Hindi
ध्यान दें– प्रिय दर्शकों Karak in Hindi Grammar ( Article ) आपको अच्छा लगा तो जरूर शेयर करे।